Sem 1 (unit 1) शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य एवं क्षेत्र
शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य एवं क्षेत्र
Aims, Objectives & Scope of Physical Education
शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य
शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में जानने से पहले लक्ष्य एवं उद्देश्य के बीच में अंतर जानना आवश्यक है।
लक्ष्य - Aim - (Ultimate Goal)
किसी कार्य को करने का अंतिम अथवा चरम उद्देश्य लक्ष्य (Ultimate Goal) लक्ष्य कहलाता है। कोई भी कार्य बिना लक्ष्य के नहीं किया जाता है।
उद्देश्य - Objectives
अंतिम लक्ष्य (Aim) प्राप्ति करने से पूर्व हमें अनेक छोटे-छोटे कार्य पूर्ण करने होते हैं जिन्हें किए बिना हम अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति की प्रक्रिया में किए जाने वाले आवश्यक कार्य जिनके बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उद्देश्य (objectives) कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए
किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतना उसका अंतिम लक्ष्य (Aim) होता है। परंतु उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक रूप से सर्वप्रथम अपने प्रदेश स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर और फिर ओलंपिक की योग्यता प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कर चयनित होना होगा तभी उसे ओलंपिक में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी। यदि वह उपरोक्त में से किसी भी स्तर असफल रहता है तो वह ओलंपिक तक नहीं पहुंच सकता।
विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। संपूर्ण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास एवं भावनात्मक विकास आते हैं। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक पक्षों के विकास के उद्देश्य पूर्ण हो जाएं।
शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Physical Education)
विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यक है
शारीरिक विकास का उद्देश्य
शारीरिक विकास शारीरिक शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थी की आयु एवं शारीरिक क्षमता के आधार पर उसके लिए विशेष प्रकार की शारीरिक क्रियाओं व खेलों का कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिससे छात्र के समस्त तंत्र जैसे परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र आदि अच्छी प्रकार विकसित हो सकें।
इसके इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है जिससे विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो सके व अपनी समस्त कार्य अच्छी क्षमता व दक्षता के साथ कार्य कर सकें व देश के लिए एक उपयोगी नागरिक बन सकें।
स्नायु-पेशीय समन्वय का विकास (Neuro-Muscular Coordination)
किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए हमारे तंत्रिका तंत्र व पेशीय तंत्र के बीच अच्छा समन्वय होना बहुत आवश्यक होता है। विभिन्न शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों व खेलों में निरंतर भाग लेने से यह क्षमता विकसित हो जाती है। अच्छे स्नायु-पेशीय समन्वय से हम लोग अपने कार्य अधिक कुशलता के साथ कर सकते हैं।
मानसिक विकास का उद्देश्य
शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों एवं खेलों में भाग लेने के लिए मानसिक सतर्कता, एकाग्रता वह सधे हुई शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य एवं अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं।
खेलों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को चतुर, तार्किक, तेजी से निर्णय लेने वाला, साहसी, स्थितियों का तुरंत आकलन करने वाला होना चाहिए जो कि अच्छे मानसिक विकास की कारण ही संभव होता है। खेलों के अभ्यास एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान छात्र के सामने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है जिसमें उसके अंदर उपरोक्त मानसिक क्षमताएं सहज रूप से विकसित होने लगती हैं।
इसके अतिरिक्त खिलाड़ी को खेल नियमों की जानकारी, खेल तकनीक का ज्ञान, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ज्ञान, संतुलित आहार की जानकारी, स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता का ज्ञान भी अति आवश्यक होता है।साथ ही खेलों में सफलता के लिए खिलाड़ी को उचित योजना एवं रणनीति बनाने की भी आवश्यकता होती है जोकि बुद्धि चातुर्य से ही संभव होता है। खेल गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेने से विद्यार्थी कि उपरोक्त सभी मानसिक क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। अतः शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों व खेलों में निरंतर भाग लेने से विद्यार्थी के मानसिक विकास की उद्देश्य की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है।
सामाजिक विकास का उद्देश्य
सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि विद्यार्थी के अंदर आवश्यक सामाजिक गुणों का विकास हो जिससे कि वह अपने समाज में बेहतर समायोजन के साथ रहे व समाज के लिए एक उपयोगी अंग बन सके।
शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम व खेलों में निरंतर भाग लेने से छात्र के अंदर निम्न सामाजिक गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है।
- खेल भावना और टीम भावना
- परस्पर सहयोग
- टीम के हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग
- नियमों का पालन करना व नियामक संस्थाओं का सम्मान करना,
- लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास
- नेतृत्व क्षमता,
- नेतृत्व के निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना,
- अपने कर्तव्यों को समझना,
- मानवीय मूल्यों का महत्व समझना,
- योग्यता का सम्मान करना
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा
- धार्मिक सद्भाव को बनाए रखना
- राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा
भावनात्मक विकास का उद्देश्य
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की सहज भावनाएं होती हैं जैसे प्रेम, समर्पण, हर्ष, दया, उत्साह, निराशा, भय, एकाकीपन, क्रोध, घृणा, कुंठा, बदले की भावना, लोभ, ईर्ष्या आदि। कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की विभिन्न भावनाएं जागृत हो सकती हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक होता है और यदि भावनाओं का प्रदर्शन आवश्यक हो तो वह नियंत्रित वह स्वीकार्य रूप में होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में छात्र को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने अथवा नियंत्रित करने के अवसर स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं जिसके फलस्वरुप छात्र भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित वह सक्षम बनता है
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र (Scope of Physical Education)
शारीरिक शिक्षा का अपना एक व्यापक क्षेत्र है। यह केवल कुछ शारीरिक क्रिया अथवा खेलों तक ही सीमित नहीं है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें कई विषयों का समावेश है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल क्षेत्र की व्यापकता निम्न विषयों के माध्यम से समझी जा सकती है
1.योग शिक्षा (Yoga)
योग विश्व कल्याण के लिए भारत का विश्व को एक अनुपम उपहार है। योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जिसे अब वैश्विक मान्यता मिल चुकी है। योग का अभ्यास व योग का अध्ययन व अध्यापन संपूर्ण विश्व में जारी है। योग शिक्षा शारीरिक शिक्षा एक दूसरे की पूरक हैं।
2.खेल समाज विज्ञान (Sports Sociology)
इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि खेल किस प्रकार सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं और खेल किस प्रकार छात्र की समाजीकरण में सहायक होता है।
3. खेल मनोविज्ञान (Sports Psychology)
इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि खेल किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और खेलों में सफलता प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान किस प्रकार सहायक होता है।
4.खेल चिकित्सा (Sports Medicine)
इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार चिकित्सा शास्त्र खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने में सहायक हो सकता है साथ ही घायल खिलाड़ियों के उपचार एवं उसकी प्रदर्शन क्षमता को वापस लाने व उसमें वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है।
5-कायिक चिकित्सा (फिजियो थेरेपी -Physiotherapy)
इसमें बिना दवाइयों का प्रयोग के केवल शारीरिक क्रियाओं व व्यायाम द्वारा रोगी की अस्थियों व पेशियों से संबंधित चोट वह बीमारियों का उपचार किया जाता है। तथा इसमें चोट और बीमारियों के कारण लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के कारण कमजोर और शिथिल पड़ गए अंगों को शारीरिक क्रियाओं एवं व्यायाम के द्वारा पुनः सबल व क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाता है।
6-खेल आहार विज्ञान (Sports Nutrition)
इसमे व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं उसके खेल प्रदर्शन पर आहार के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों की खेल व उनकी क्षमता के अनुसार उनकी आहार का निर्धारण भी किया जाता है
7-खेल दर्शन (Sports Philosophy)
इसमें खेल व शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रचलित इतिहास, परंपराओं, मान्यताओं का अध्ययन एवं विभिन्न विद्वानों द्वारा उन पर अपने व्यक्त विचार, मत, टीका, टिप्पणिओं, समालोचनाओं की विवेचना की जाती है।
8-खेल प्रबंधन (Sports Management)
इसके अंतर्गत खेल व शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन से जुड़े हुए कार्य जैसे खेल प्रतियोगिता का आयोजन, संस्थाओं में खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, खेल बजट, खेल कैलेंडर का निर्माण, खेल सुविधाओं का निर्माण आदि का क्रियान्वयन किया जाता है।
9-खेल इंजीनियरिंग (Sports Engineering)
यह विभिन्न प्रकार के खेल उपकरणों का निर्माण, खेल सुविधाओं जैसे ट्रैक, खेल मैदान, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम आदि का निर्माण आदि से संबंधित क्षेत्र है
10-खेल पत्रकारिता (Sports Journalism)
यह खेलों की मीडिया कवरेज से संबंधित क्षेत्र है। इसमें अखबारों व मैगजीन में खेलों की रिपोर्टिंग, खबरों व आर्टिकल का लेखन, खेल प्रतियोगिताओं का सजीव प्रसारण, कमेंट्री, खिलाड़ियों का इंटरव्यू जैसे कार्य आते हैं
11-खेल यांत्रिकी (खेल बायोमैकेनिक्स Sports Biomechanics)
इसमें खेलों के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा की जाने वाली गतियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों की तकनीक में अपेक्षित सुधार लाकर उनके प्रदर्शन को बेहतर करना होता है।
12- खेल फैशन डिजाइनिंग (Sports Fashion Designing)
खिलाड़ियों के उपकरण व उनकी पोशाक उनके खेल प्रदर्शन को बेहतर करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है, इस बात का अध्ययन खेल फैशन डिजाइनिंग में किया जाता है।
13- दिव्यांग लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल (Para Sports)
इसमें कुछ विशेष प्रकार से सक्षम खिलाड़ियों (Differently Abled Athletes) हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन व उनके लिए विशेष उपकरण व सुविधाओं के निर्माण का अध्ययन किया जाता है।
14- खेल एजेंट (Sports Agents)
आधुनिक खेल संस्कृति के अंतर्गत यह अपेक्षाकृत एक नया क्षेत्र है। खेल एजेंट वे लोग होते हैं जो प्रसिद्ध खिलाड़ियों के खेल एवं खेल के अतिरिक्त व्यवसायिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
15- इवेंट मैनेजर (Event Manager)
इवेंट मैनेजर वे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो एक निर्धारित शुल्क लेकर किसी बड़े खेल कार्यक्रम अथवा खेल प्रतियोगिता को आयोजित कराने हेतु संपूर्ण तकनीकी विशेषज्ञता एवं लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध कराते हैं।
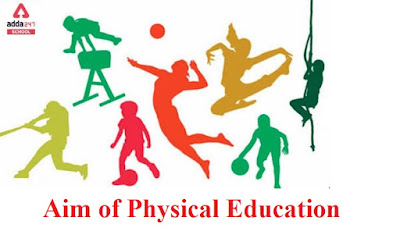



Comments
Post a Comment